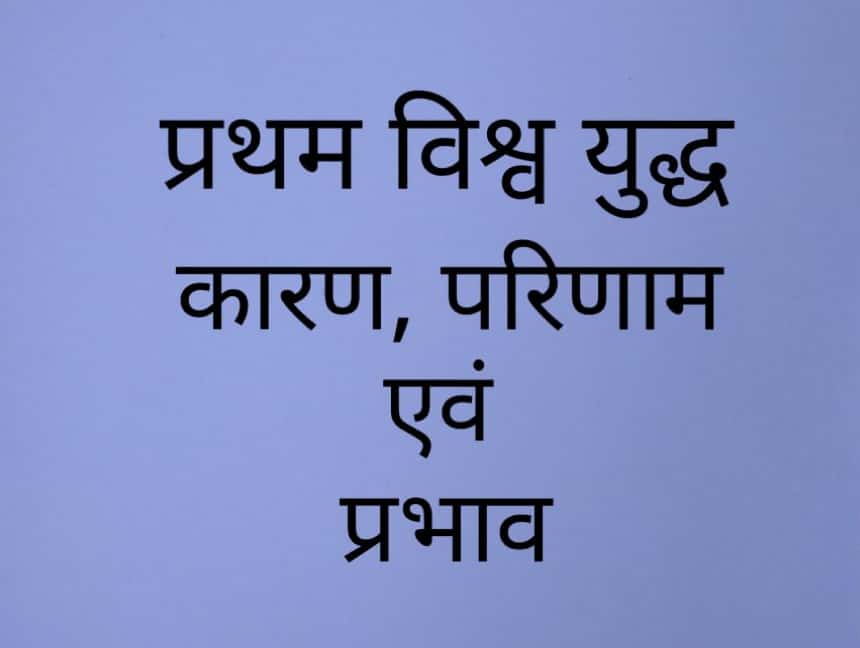प्रथम विश्व युद्ध –
प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था. प्रथम विश्व युद्ध यूरोप का व्याप्त महायुद्ध था. इसमें विश्व के कुल 36 देशो ने भाग लिया जिस कारण इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है।
युद्ध मे सम्मिलत राज्य –
मित्र राष्ट्र – इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान, इटली, सर्बिया, पुर्तगाल, रूमानिया, चीन, भारत, क्यूबा, पनामा, ब्राजील, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका।
धुरी राष्ट्र – जर्मनी, आस्ट्रिया – हंगरी, टर्की तथा बल्गेरिया।
● प्रथम विश्व युद्ध के कारण –
प्रथम विश्व युद्ध का आरम्भ 1914 ईस्वी में आस्ट्रिया के युवराज फर्डी नेण्ड की हत्या के कारण हुआ था. किन्तु यह कोई आकस्मिक घटना नही थी. इसकी पृष्ठभूमि 1870 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक यूरोपीय राज्यो के स्वार्थो, नीतियों तथा घटनाओं द्वारा तैयार हो चुकी थी।
प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है.
(क) आधारभूत कारण
(ख) अंतरराष्ट्रीय संकट
(ग) तात्कालिक कारण
(क) आधारभूत कारण –
गुप्त संधिया तथा गुटबन्दी – प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण गुप्त संधियों से उतपन्न गुटबन्दी थी. इसकी शुरुआत प्रशा के हाथों फ्रांस की पराजय से हुई. एकीकृत जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रतिशोध की भावना ग्रस्त फ्रांस को मित्रहीन बनाये रखना था. इसके लिए उसने 1879 ईस्वी में आस्ट्रिया के साथ गुप्त संधि द्वारा द्वि-गुट का निर्माण किया. उसने 1882 ईस्वी में इटली को भी सम्मिलित करते हुए त्रिमैत्री संधि द्वारा फ्रांस एवं रूस के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण किया. अक्टूबर 1883 ईस्वी में बिस्मार्क ने जर्मनी, आस्ट्रिया तथा रुमानियका से त्रिपक्षीय गठजोड़ स्थापित किया. बिस्मार्क ने आस्ट्रिया से छिपते हुए 1887 ईस्वी में रूस के साथ पुनआष्वासन की संधि कर ली, ताकि रूस फ्रांस की ओर उन्मुख न हो सके. 1890 ईस्वी में बिस्मार्क के त्याग पत्र के साथ ही जर्मनी की विदेश नीति में आमूल-चूल परिवर्तन होने लगा. जमनी द्वारा बाल्कन प्रदेश में आस्ट्रिया के समर्थन से अप्रसन्न रूस तथा फ्रांस के बीच 1894 ईस्वी में मैत्री संधि हो गई. अब तक एकाकी इंग्लैंड ने जर्मनी से मित्रता के प्रयास किए लेकिन इंग्लैंड लक्ष्य में सफल नही हो सका. जर्मनी की महत्वकांक्षा को देखते हुए इंग्लैण्ड ने अपने पुराने शत्रु फ्रांस से मतभेद दूर करने आरम्भ कर दिए. 1904 ईस्वी में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच दोस्ती हो गई. 1904 ईस्वी में इंग्लैंड तथा रूस में संधि हो गई. इस प्रकार सम्पूर्ण यूरोप दो गुटों में विभाजित हो गया. इन गुप्त संधियों तथा गुटों ने परस्पर तनाव तथा स्पर्धा को बढ़ावा दिया. गुट में सम्मिलित राज्य स्वयं का हित न होते हुए भी मित्र राज्य का सहयोग करने हेतु वचनबद्ध था।
शस्त्रीकरण तथा सैन्यवाद – 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में यूरोप में सैन्य वाद तथा शस्त्रीकरण की स्पर्धा आरम्भ हुई. पूर्व में सैनिक शक्ति को आधार बनाकर जर्मनी ने आस्ट्रिया तथा फ्रांस को पराजित किया था. अब फ्रांस ने पराजय का प्रतिशोध लेने हेतु सैनिक शक्ति में व्रद्धि करना आरम्भ कर दिया. जापान से पराजित रूस ने भी सैनिक शक्ति बढ़ाना आरम्भ कर दिया. 1890 ईस्वी के पश्चात जर्मनी ने नौ सेना का विस्तार तेजी से किया. इसे चुनौती मानकर इंग्लैंड ने भी नौ सेना व्रद्धि आरम्भ कर दी. यही नही सैन्यवाद तथा शस्त्रीकरण की इस स्पर्धा से शासन में सैनिक अधिकारियों का वर्चस्व बढ़ने लगा।
उग्र राष्ट्रवाद – राष्ट्रीयता की भावना फ्रांसिसी क्रांति की देन थी. कालांतर में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ. इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी तथा इटली के एकीकरण हुआ. लेकिन 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रीयता की इस भावना ने उग्र रूप धारण कर लिया. प्रत्येक राष्ट्र अपने विस्तार, सम्मान तथा गौरव की व्रद्धि तथा अन्य देशों को नष्ट करने को उद्यत हो उठे।
आर्थिक एवं औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा – आर्थिक एवं औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा प्रथम विश्व युद्ध का कारण थी. 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध तक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान तथा अमेरिका का तेजी से औधोगिक विकास आरम्भ हुए. इसके साथ ही कच्चे माल की आपूर्ति तथा उत्पादिक माल के लिए नवीन बाजारों की आवश्यकता हुई. बढ़ती जनसंख्या तथा सैनिक आवश्यकताओं ने भी उपनिवेश स्थापना हेतु प्रेरित किया. इन प्रतिस्पर्धा में सवार्धिक क्षेत्र इंग्लैंड तथा फ्रांस को प्राप्त हुआ. जर्मनी इसमें पीछे रह गया. 1890 ईस्वी के बाद उसने उपनिवेश प्राप्ति के प्रयास आरम्भ किए. जिससे इंग्लैंड तथा फ्रांस उसके शत्रु हो गए. रूस तथा आस्ट्रिया ने बाल्कन प्रदेश में प्रभाव बढ़ाना आरम्भ कर दिया. इटली भी उपनिवेशों के लिए लालायित था. उपनिवेश प्राप्ति की इस स्पर्धा ने परस्पर घ्रणा तथा अविश्वास को बढ़ाया।
समाचार पत्र तथा युद्धोंन्मादी प्रचार – यूरोपीय देशो के बीच द्वेष, शत्रुता तथा युद्धोंन्मादी को बढ़ाने में तत्कालीन समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. इंग्लैंड के समाचार पत्र जर्मनी सम्राट की नीतियों की आलोचना कर रहे थे. तो दूसरी ओर जर्मनी समाचार पत्र फ्रांस तथा इंग्लैंड के प्रति कटुतापूर्ण लेख प्रकाशित कर रहे थे. आस्ट्रिया के युवराज की हत्या के बाद आस्ट्रिया तथा सर्बिया के समाचार पत्रों ने एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने वाले लेख प्रकाशित किए. इस काल के दार्शनिक तथा विचारको ने युद्ध को राष्ट्र की उन्नति के लिए अपरिहार्य बताया. इनमें दार्शनिक हीगल तथा माल्थस प्रमुख है. विश्व पर वर्चस्व स्थापना हेतु लालायित राष्ट्रों में इनमें विचार अत्यधिक लोकप्रिय होने लगे।
अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव – इस समय किसी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता थी, जो यूरोपीय राज्यों के आपसी विवादों का हल निकालकर उन्हें युद्ध से विमुख कर देती. लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी संस्था नही होना भी इस विश्व का एक कारण था।
(ख) अंतर्राष्ट्रीय संकट –
रूस जापान सघर्ष (1904-05) – रूस तथा जापान के बीच संघर्ष में जापान जैसे छोटे से एशियाई देश ने यूरोप की महाशक्ति रूस को बुरी तरह पराजित कर दिया. इस पराजय ने रूसी साम्राज्य की सुदूर पूर्व में विस्तारवादी महत्वकांक्षा को रोक दिया. विवश रूस ने अब बाल्कन क्षेत्र में रुचि लेना आरम्भ कर दिया. यहाँ उसके हस्तक्षेप ने जर्मनी को आस्ट्रिया तथा टर्की का पक्ष लेने हेतु बाध्य कर दिया. यही नही रूस की पराजय का प्रभाव फ्रांस की स्थिति पर भी पड़ा. अब जर्मनी ने मोरक्को का पक्ष लेकर फ्रांस को चुनौती देना प्रारम्भ कर दिया।
मोरक्को संकट – अफ्रीका के उत्तर में स्थिति मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया फ्रांस के नियंत्रण में थे. 1905 ईस्वी में जर्मनी के सम्राट ने मोरक्को की यात्रा की तथा मोरक्को की अखंडता तथा स्वतन्त्रता की घोषणा की. फ्रांस ने इसका विरोध किया।
बोस्निया तथा हर्जगोविना विवाद – इन दोनों प्रदेशो में सर्व जाति के लोग रहते थे. 1878 ईस्वी की बर्लिन कांग्रेस में इन प्रदेशो पर शासन करने का अधिकार आस्ट्रिया को दिया गया था. इन दोनों प्रदेशों की जनता सर्बिया में विलय चाहती थी. 6 अक्टूबर 1908 ईस्वी को आस्ट्रिया ने इन प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिला लिया. फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, सर्बिया तथा रूस ने आस्ट्रिया के इस कदम की कड़ी आलोचना की. इस प्रश्न पर सर्बिया तथा रूस द्वारा आस्ट्रिया पर आक्रमण की आशंका उत्पन्न हो गई. जर्मनी ने आस्ट्रिया का पक्ष लिया. यह संकट तो टल गया लेकिन आस्ट्रिया के इस कार्य से सर्बिया में आस्ट्रिया विरोधी भावनाएं बढ़ने लगी।
अगाडीर संकट – 1911 ईस्वी में फ्रांस ने मोरक्को में शांति स्थापना हेतु अपनी सेनाएं भेजी. जर्मनी ने इसका विरोध करते हुए मोरक्को में जर्मनी हितों की रक्षा हेतु अपने युद्धपोत पैंथर को मोरक्को के बन्दरगाह अगाडीर में भेज दिया. इस घटना ने जर्मनी तथा फ्रांस के बीच युद्ध का खतरा उपस्थित कर दिया।
बाल्कन युद्ध (1912-13 ईस्वी) – बाल्कन युद्ध ने यूरोपीय राज्यों के मध्य कटुता बढ़ाने का कार्य किया. युद्ध के पश्चात लन्दन सम्मेलन भी बाल्कन राज्यों के विवाद हल करने में असफल रहा. इस सम्मेलन द्वारा आस्ट्रिया के जोर डालने पर अल्बानिया की स्थापना की गई. इससे सर्बिया की समुन्द्र तट प्राप्ति की लालसा को धक्का लगा. अब सर्बिया में आस्ट्रिया का विरोध और भी बढ़ गया. रूस द्वारा सर्बिया की मांग का समर्थन किए जाने से दोनों के मध्य मैत्री बन्धन को दृढ़ता मिली. इस सम्मेलन के निर्णयों से सबसे अधिक हानि बल्गारिया को हुई. सम्मेलन के निर्णयों से अप्रसन्न बल्गारिया विवश होकर जर्मनी की ओर झुकने लगा. लन्दन सम्मेलन के निर्णयों से निराश टर्की भी अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु जर्मनी की शरण में चला गया. वास्तव में बाल्कन युद्ध के परिणामों ने शस्त्रीकरण तथा गुटबन्दी को प्रोत्साहन दिया. ग्रांट एवं टेम्परले के अनुसार “प्रथम विश्वयुद्ध के लिए कोई घटना इतनी अधिक उत्तरदायी नही है जितनी कि बाल्कन युद्ध।”
(ग) तात्कालिक कारण –
आस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेण्ड की हत्या – 29 जून 1914 ईस्वी को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में आस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेण्ड तथा उनकी पत्नी की दो सर्ब युवको ने सरे आम सड़क पर हत्या कर दी. दोनों हत्यारे सर्व स्लाव आंदोलन से संबंधित थे. इस हत्याकांड की आस्ट्रिया में कड़ी प्रतिक्रिया हुई. हत्यारे सर्ब होने के कारण आस्ट्रिया ने सर्बिया को कठोर दण्ड देने का निश्चय किया. आस्ट्रिया को जर्मनी का समर्थन प्राप्त था. 23 जुलाई 1914 ईस्वी को आस्ट्रिया ने कठोर शर्तो सहित सर्बिया को अल्टीमेटम दिया. आस्ट्रिया ने इसे 48 घण्टे में स्वीकार न करने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी. यधपि कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र इसे स्वीकार नही कर सकता था. फिर भी निर्धारित अवधि में सर्बिया ने अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली. लेकिन आस्ट्रिया युद्ध करने पर उतारू था. 28 जुलाई 1914 ईस्वी को आस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी. 30 जुलाई को रूस ने सर्बिया के पक्ष में लामबन्दी की घोषणा कर दी. 1 अगस्त को जर्मन ने रूस के विरुद्ध तथा 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया. जर्मन सेनाओं के बेल्जियम में घुसते ही इंग्लैंड ने भी 4 अगस्त को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया. 23 अगस्त को जापान तथा 29 अक्टूबर को टर्की भी युद्ध मे सम्मिलित हो गया।
● प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम एवं प्रभाव –
इस महायुद्ध में 36 देशो ने भाग लिया. यह युद्ध 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक चला. परवर्ती युग में प्रत्येक क्षेत्र में इसके परिणाम एवं प्रभाव दिखाई दिए।
जन धन की अपार हानि – प्रथम विश्व युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग साढ़े छः करोड़ सैनिकों ने भाग लिया. इसमें से 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गए. 2 करोड़ 20 लाख सैनिक घायल हुए. इनमें से 70 लाख सैनिक अपाहिज हो गए. बड़ी संख्या में हत्याकांडों, भुखमरी, बीमारी से लोग मारे गए. दोनों पक्षों ने इस युद्ध पर एक खरब छियासी अरब डॉलर खर्च किए।
निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति – इस विश्व युद्ध ने जर्मनी, रूस, आस्ट्रिया तथा टर्की के निरंकुश राजतंत्रों को समाप्त कर दिया. अब इन देशों में जन प्रतिनिधि शासन की स्थापना हुई।
नवीन राज्यों का उदय – इस महायुद्ध के पश्चात शांति संधियों द्वारा विश्व मानचित्र पर अनेक परिवर्तन किए गए. चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, लिथुआनिया, लेटविया, एस्टोनिया, फ़िनलैंड, पॉलैंड आदि नये राज्यों का उदय हुआ. इन सभी राज्यों में लोकतन्त्रात्मक शासन स्थापित किए गए।
संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में व्रद्धि – प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप अमेरिका की शक्ति तथा राजनीतिक प्रभाव में व्रद्धि हुई. युद्ध मे ही नही बल्कि शांति सम्मेलन में भी अमेरिका राष्ट्रपति विल्सन की अहम भूमिका रही. युद्ध में अमेरिका ने मित्रराष्ट्रों को बड़ी मात्रा में ऋण देकर स्वयं को आर्थिक महाशक्ति प्रमाणित किया।
शस्त्रीकरण – प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात निश:स्त्रीकरण के स्थान पर शस्त्रीकरण की स्पर्धा को प्रोत्साहन मिला. युद्ध के दौरान एक ओर विजयी राष्ट्र प्राप्त किए गए लाभों को बनाये रखने हेतु तो दूसरी ओर पराजित राष्ट्र खोए हुए सम्मान को पुनः पाने एवं प्रतिशोध भावना से शस्त्रीकरण करने लगे।
राष्ट्रसंघ की स्थापना – प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव था. जो कि युद्ध को टालने के लिए प्रयास कर सकती थी. अमरीकी राष्ट्रपति के आग्रह पर राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई. यह संस्था यधपि अपने उद्देश्य में सफल सिद्ध नही हुई किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह नवीन प्रयोग अवश्य था।
Tags: 1st world wor reason results and efact, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध किन देशो में लड़ा गया, प्रथम विश्व युद्ध के कारण परिणाम एवं प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ